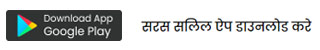‘तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो घूमने के कभीकभी ही अवसर मिलते हैं,’ शांता का रोषपूर्ण स्वर था.
और अधिक सुनने का साहस न था दीनानाथजी में. सो, कमरे का दरवाजा बंद कर हाथ की किताब रख दी और बत्ती बुझा कर सोने की चेष्टा करने लगे. किंतु कहां थी नींद आंखों में? बंद भीगी पलकों में वे सुनहरे छायाचित्र तैर रहे थे, जो पत्नी के साथ बिताए 40 वर्षों की देन थे.
अपना एकाकीपन आज उन्हें बुरी तरह झकझोर गया. फिर भी स्वाभिमान के धनी थे. इसलिए सुबह होते ही सुकांत से अपने वापस जाने की इच्छा प्रकट की. किंतु सुकांत अटल था अपने निश्चय पर कि बाबूजी यहीं रहेंगे. सो, वे वहीं रहे. सुकांत अकेला ही जरमनी गया. सुकांत के बिना वह पूरा 1 महीना दीनानाथजी ने लगभग मौनव्रत रख कर ही काटा.
और फिर एक दिन उन के दांत में बेहद दर्र्द होने लगा. सारा दिन दर्द से तड़पते रहे. अपने देश में तो दंतचिकित्सक था, जो एक फोन करते ही उन्हें आ कर देख जाता था. दवा तक खरीदने जाना नहीं पड़ता था. वही खरीद कर भिजवा देता था. किंतु यहां? यहां तो वे असहाय से मफलर से मुंह लपेटे दफ्तर से सुकांत के घर लौटने का इंतजार करते रहे. यहां न तो वे गाड़ी चला सकते थे और न ही उन्हें किसी डाक्टर का पता मालूम था.
शाम को सुकांत लौटा तो बाबूजी का सूजा हुआ गाल देख कर सब समझ गया. पिता को गाड़ी में बिठा कर तुरंत दंतचिकित्सक के पास ले गया. 80 डौलर ले कर डाक्टर ने उन्हें देखा और फिर आगे के स्थायी इलाज के लिए लगभग 3,000 डौलर का खर्चा सुना दिया. दवा आदि ले कर जब सुकांत बाबूजी के साथ घर लौटा तो उस का चेहरा खिलाखिला सा था कि बाबूजी को अब आराम आ जाएगा.
आगे की कहानी पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें
डिजिटल
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
डिजिटल + 24 प्रिंट मैगजीन
सरस सलिल सब्सक्रिप्शन से जुड़ेें और पाएं
- सरस सलिल मैगजीन का सारा कंटेंट
- 1000 से ज्यादा सेक्सुअल हेल्थ टिप्स
- 5000 से ज्यादा अतरंगी कहानियां
- चटपटी फिल्मी और भोजपुरी गॉसिप
- 24 प्रिंट मैगजीन